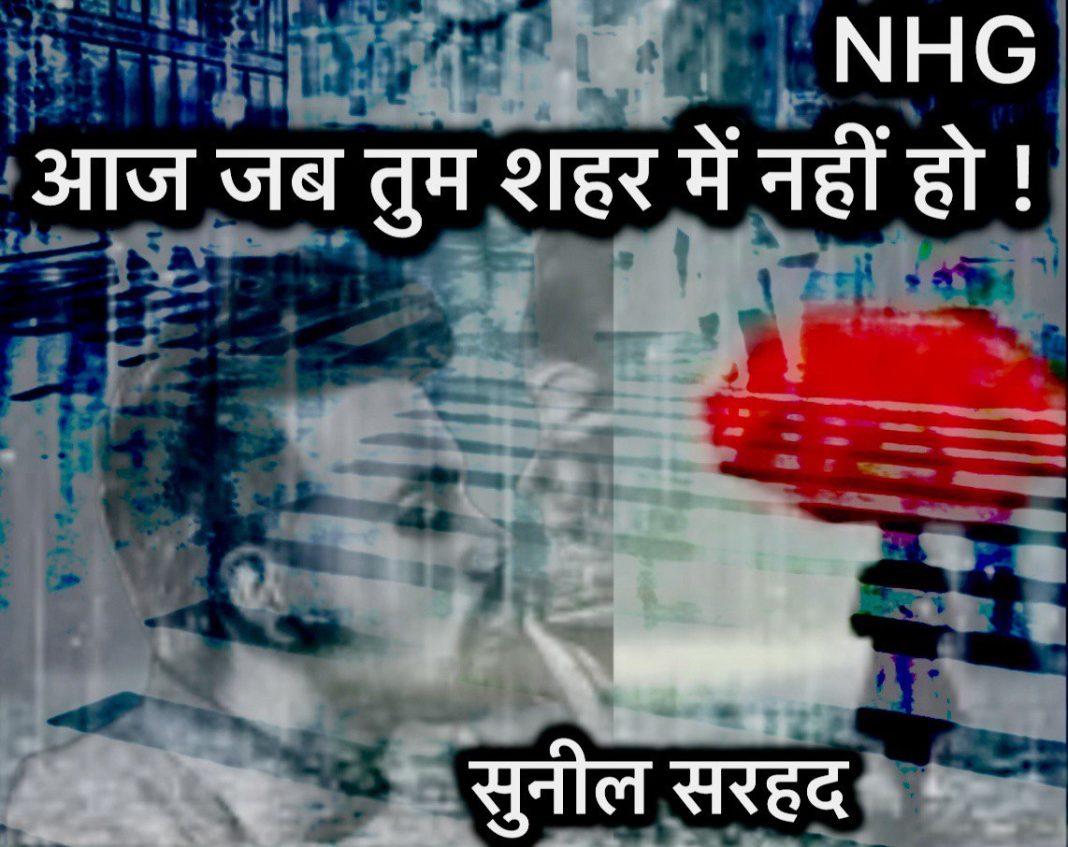वह एक दिसंबर की शाम तनिक मेहरबान हो आई जब नेटफ्लिक्स पर रैंडम सर्च के दौरान कला का
पोस्टर दिख आया, “बुलबुल” जैसी डिसास्टर फिल्म की निर्देशक अन्विता दत्ता का नाम पढ़कर थोड़ी झिझक ज़रूर हुई लेकिन निर्माता लिस्ट में शामिल अनुष्का शर्मा ने प्ले क्लिक करवा दम लिया।
इसके पूर्व अनुष्का शर्मा की बांग्लादेश में कुचलित शैतानिक पंथ पर आधारित फिल्म ‘परी‘ ने स्तब्ध किया था। मैं उनकी बूझ पर चौंक सी गई थी। ऐसी ऑफ बीट, नॉन कमर्शियल फिल्म में पैसा लगा उन्हें क्या ही हासिल हुआ होगा ? एक दूसरा और प्रश्न अडिग हो आया था कि दिल्ली के आधुनिक परिवेश में पली पढ़ी बांग्लादेश की विलुप्त औलादचक्र कुप्रथा में इफ्रीत की बेटी पिशाचनी बनना क्यों पसंद किया जबकि आजकल हमारे बुजुर्गवार अदाकार युवाओं को टक्कर देने के जोश से भरे हुए हैं। ख़ैर, परी इतनी पसंद आई थी कि स्वयं को कला देखने से रोक नहीं पाई और यक़ीन मानिए देखने के बाद महीनों फ़िल्म से ख़ुद को अलग कर पाना मुश्किल रहा!
प्रथम फ़िल्म के टाइटल पर बात करें तो Qala एक अरेबिक शब्द है जिसका हिन्दी अर्थ दुर्ग या कि क़िला है, 2008 में इसी नाम से एक अज़रबैजानिक फ़िल्म आई थी, सब टाइटल था “द कैसल”, जैसा कि नाम से ही बज़ाहिर है फ़िल्म में क़िला स्वयं एक चरित्र है और तमाम घटनाओं का गवाह, जबकि हिन्दी फ़िल्म कला, मुख्य भूमिका में कला नामक स्त्री और संगीत के बारे में है तो कई मर्तबा मुझे लगता है अगर फ़िल्म का टाइटल qala न होकर kala रहता तो सायास ही जुड़ाव मुमकिन था किंतु तब संभव है फ़िल्म को हम तुरंत ही कालेपन से जोड़कर देखते जो संभवतः उचित नहीं रहता !
कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो गायिकी के क्षेत्र में सफलता के शीर्ष पर पहुँच कर आत्महत्या कर लेती है। वास्तव में कला उपेक्षा और अपेक्षा में मध्य द्वंद्व की ऐसी मनोवैज्ञानिक कहानी कहती है जो आपको बेचैन करती है। दिन-रात का सुकून छीन लेती है,ठहर कर सोचने को विवश करती है कि क्यों हम बच्चों के कंधे पर अपनी उम्मीदों का भारी बोझ डाल देते हैं कि उसमें दब कर उनका दम निकल जाता है। साधारण तरीके से या मात्र एक फ़िल्मी क्रिटिक के नज़रिए से देखने पर आप मोरल या कि सामाजिक सन्देश इत्यादि में उलझ कर रह जाते हैं और आपकी आँखों से ओझल रह जाता है दृश्यों का कोलाज, भावनाओं का झंझावात, ऊहापोह और भीतरी द्वन्द जो फ़िल्म में अनवरत चलता रहता है जहाँ कला माँ के लिए गाना चाहती है वहीं जगन इसलिए गाता है कि वह गाए बग़ैर जी नहीं सकता !
एक संवेदनशील मनुष्य कला के दर्द से चूक नहीं सकता; माँ के प्रेम अभाव से जनित दर्द जिसकी अजस्र पीड़ा कला को अहर्निश तड़पाती है | आम तौर पर देखने पर लगता है वह गायिका बन प्रसिद्धि पाना चाहती है जबकि वह सिर्फ माँ का प्रेम चाहती है। वह चाहती है कमी रह जाने पर भी एक बार माँ उसे अपने कलेजे लगाये और कहे “कला तुमने बहुत बेहतर किया” जबकि उसकी माँ उसे बर्फ गिरती रात घर के बाहर कर देती है। माँ के क्रोध के साये में कलपती कला कभी संगीत की कला में दक्ष नहीं हो पाई और माँ ने प्रखर, प्रवीण युवक को बेटा अपना लिया और कला को उसकी चाकरी में नियुक्त कर दिया जो उसे पुरुष की नज़र से देखता है यह बात कला से छुपी नहीं अतः वह माँ से कहती है मेरी उससे शादी करा दो किंतु माँ ने डपट दिया। दरअसल माँ परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बेटा चाहती थी, एक बार वह कला से कहती भी हैं ” तुम सीख सकती हो संगीत, लड़की होकर भी” !
कला के दुर्दम्य महत्त्वाकांक्षा को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना तिरस्कार से उपजी कुंठा को जान लेना | स्त्री देह होने की कुंठा, माँ की तरह न हो पाने की कुंठा के बाद दत्तक भाई से कमतर होने की कुंठा, कला कुंठा का पुंज बन गई थी जो उसके भीतर विषबेल की सी चढ़ती जा रही थी। इतनी कि वह दत्तक भाई के दूध में पारा मिला देती है और इस अपराधबोध से कभी मुक्त नहीं हो पाई !
दत्तक पुत्र द्वारा मृत पति की गायकी की परंपरा को आगे ले जाने हेतु माँ के प्रपंचों से सीखती कला स्वयं को सिद्ध करने हेतु देह की सौदेबाजी तक से गुरेज नहीं करती | ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर से ग्रसित माँ के प्रेम को तरसती समझौते करती कला संगीत का सबसे बड़ा सम्मान तो हासिल कर लेती है किन्तु तब भी माँ का प्रेम हासिल नहीं। दरअसल माँ ने कला से कभी प्रेम किया ही नहीं और कला उनसे सिर्फ़ प्रेम चाहती रही इसके लिए उससे जो बन पड़ा उसने वह किया!
व्यावसायिक दृष्टि से फ़िल्म की सफलता को आंकने का एक ही पैमाना है “कमाई कितनी हुई?” किंतु कई सारी फ़िल्में अपने कंटेंट, परफॉरमेंस और कथानक के दम पर बर्षों बरस तक दर्शक के दिल और दिमाग़ पर छाई रहती है, कला उनमें से एक है। इसे मात्र एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फ़िल्म की तरह देख पाना संभव नहीं, कला सिनेमेटोग्राफ़ी का उत्कृष्ट नमूना है, दरअसल कला एक उन्नत सिनेमाई कलाकृति है!
1940 के फ्रेम में सजी यह फ़िल्म दृश्य दर दृश्य उजागर होती है, चाहे वह माँ का बेटे के लिए ललक हो या बेटी पर कठोर शासन या कि अंकुश। हिमाचली बैकग्राउंड आधारित यह फ़िल्म तमाम वक़्त अपनी छाप लिए दिखती है, गहने, कपड़े या घर के फ़र्नीचर, गिरता बर्फ या अंधेरे और रोशनी का खेल जो समूची फ़िल्म पर तारी रहता है! कई दृश्यों में शिवानी की सात फेरे याद हो आती है, असल में कथा बुनावट में भी, बहुत सारा हिमाचल और थोड़ा सा कलकत्ता। कहानी इतनी महीनता से बुनी गई है कि एक मामूली चूक की गुंजाइश नहीं किंतु कभी -कभी लगता है काश माँ का चरित्र जरा और खुलता, थोड़ा और स्पष्ट होता तब शायद कला का चरित्र का ग्रे शेड इतना निखर कर नहीं उभरता!
लैला-मजनू से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली तृप्ति दमरी फिल्म शुरू होते ही आपको मोहविष्ट कर लेती हैं, तमाम दृश्यों को वह ऐसे ऐसे उठाती हैं मानो यह उसकी अपनी कहानी है, शीर्षस्थ पक्व गायिका बरतते हुए वह एक क्षण को भी कमज़ोर नहीं पड़ती, वहीँ दूसरी ओर एक कमतर, कुंठित, स्थापित होने को ललायित कला के चेहरे के भाव उतने ही बेगुनाह हैं जितनी कि वह स्वयं! यद्यपि बार-बार हाथ धोकर वह दूध में पारा मिलाने के पाप से मुक्त होना चाहती है किन्तु काश कि एक बार माँ अपनी गोद में उसका सिर धर बालों को सहलाती। समूची फिल्म में “अपेक्षा और उपेक्षा के मध्य का द्वन्द भाव” सतत दरिया-सा निरंतर बहता रहता है |
फिल्म का चलचित्रण इतना मनोहारी है कि आप एक दृश्य भी स्किप नहीं करना चाहेंगे जैसा कि अमूमन हम करते रहा करते हैं। कई दृश्य, कम्पोजीशन में इतने लुभावने बन पड़े हैं कि आप पॉज कर निहारते हैं, उस दृश्य को अपनी दीवार पर टाँकना चाहते हैं। फिल्म देखते हुए आप कला की पीड़ा से स्वयं को अलग नहीं रख पाते हैं, वह एक द्वन्द आपके भीतर भी अनवरत चलता है, आप मुक्त नहीं रह पाते …आप दृश्यों के साथ -साथ चलते हैं, आप भी कला के दुःख में डूबते-उतरते हैं। इतने कि माँ को उसका फेक कॉल फ़ौरन ही बूझ लेते हैं!
स्वस्तिका मुखर्जी कितनी ही मर्तबा मन्दाकिनी होने का भ्रम पैदा करती है, कला का तिरस्कार करती माँ निबाहती उर्मिला मंजुश्री से आप घृणा नहीं कर पाते, वह दृश्य-दर-दृश्य इतनी सहजता से अपनी पीड़ा का यक़ीन दिलाती जाती है कि आप अंततः कला को ही अपराधी मान लेते हैं |
जीवन में माँ के प्रेम के महत्त्व पर कार्ल उंग कहते हैं – “सभी तरह के बढती और परिवर्तन की रहस्यमयी जड़, वह प्यार जिसका अर्थ है घर वापसी, आश्रय और लम्बी चुप्पी जिससे सब कुछ शुरू होता है सब कुछ समाप्त होता है”।
कला भी समाप्त हो जाती है |
कई दूसरे गीतों की धुन सुनाई के देने के बाबजूद गीत संगीत की मिठास जुबां पर घुल सी गई है !!!
प्रियंका ‘ओम’